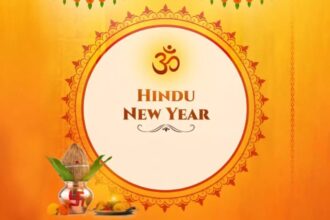आज यानी 2 अप्रैल को पूरे विश्व में “विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस” के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिन को विशेष रूप से Autism Spectrum Disorder के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्धारित किया। यह दिन उन लाखों बच्चों और वयस्कों की आवाज़ बनने का एक अवसर है जो ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं और समाज में जुड़ाव की आवश्यकता महसूस करते हैं।
ऑटिज्म क्या है? कैसे होता? इस बारे में ढेरों लेख मिल जायेंगे इसलिए इस लेख में हम बताएंगे की ऑटिस्टिक व्यक्तियों की देखभाल कैसे की जाए और कैसे उन्हें समाज का हिस्सा बनाया जाये?
ऑटिज्म एक न्यूरोडेवलपमेंटल विकार है, जो व्यक्ति के social behaviour, sensory responses को प्रभावित करता है। दुनिया भर में लाखों लोग ऑटिज्म से प्रभावित हैं, और सही देखभाल व समर्थन से वे भी एक सुखद, आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं।
ऑटिस्टिक व्यक्तियों को केवल “बीमार” या “अलग” मानने के बजाय, हमें उनकी अनूठी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। सही देखभाल और समावेश से उनका जीवन आसान बनाया जा सकता है।
सबसे पहले तो बच्चे के परिवार को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। माता-पिता और भाई-बहनों को ऑटिज्म के लक्षणों, जरूरतों और संभावित चुनौतियों को समझने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए।
कई ऑटिस्टिक बच्चे और वयस्क बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में माता-पिता को उनके साथ संवाद करने के वैकल्पिक तरीके खोजने चाहिए, जैसे कि इशारे, चित्रों का उपयोग, या Augmentative and Alternative Communication devices. बातचीत के दौरान छोटे, सरल वाक्य प्रयोग करें और धैर्यपूर्वक उनके जवाब देने का इंतजार करें।
उनकी दिनचर्या में स्थिरता बनाए रखें, क्योंकि ऑटिस्टिक व्यक्ति अचानक बदलाव से असहज हो सकते हैं। घर में एक शांत वातावरण बनाएं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी शोर-शराबे से बचाने के लिए हेडफोन या अन्य सहायता दें।
ऑटिस्टिक बच्चों के लिए विशेष शिक्षा स्कूलों या समावेशी स्कूलों में ट्रेनिंग ले चुके शिक्षकों की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे हर बच्चे की क्षमता और सीमाओं के आधार पर अनुकूल शिक्षण के तरीके अपनाएँ।
कंप्यूटर प्रोग्राम, टचस्क्रीन डिवाइसेज़ और वॉयस-टू-टेक्स्ट टेक्नोलॉजी जैसे टूल्स ऑटिस्टिक बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। चित्रों और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई अधिक प्रभावी हो सकती है।
स्कूलों में ऑटिस्टिक बच्चों को सामाजिक बातचीत और समूह गतिविधियों में शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अन्य छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे ऑटिस्टिक बच्चों को दोस्ती और सहयोग प्रदान कर सकें।
ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से autism-friendly workplaces की व्यवस्था की जानी चाहिए। कंपनियों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्तियों की क्षमताओं के अनुसार कार्य अवसर प्रदान करें, जैसे कि डेटा एनालिसिस, कला, डिजाइन, लेखन, प्रोग्रामिंग आदि।
ऑटिस्टिक बच्चों और वयस्कों को खेल, संगीत, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सामुदायिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।
मॉल, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर quiet zones बनाए जाने चाहिए ताकि ऑटिस्टिक व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर वहां आराम कर सकें। मेडिकल सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं में भी ऐसे व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
जिन ऑटिस्टिक बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है, उनके लिए स्पीच थेरेपी बहुत फायदेमंद हो सकती है। Applied Behavior Analysis से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।
ऑटिस्टिक व्यक्ति भी डिप्रेशन और चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता ज़रूरी है। माता-पिता और देखभाल करने वालों को भी काउंसलिंग मिलनी चाहिए ताकि वे धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभाल सकें।
कई माता-पिता को यह लगता है कि वे इस चुनौती में अकेले हैं। लेकिन विभिन्न NGO और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स से जुड़कर वे दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं।
लगातार देखभाल करने की वजह से माता-पिता मानसिक और शारीरिक रूप से थक सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए।
ऑटिस्टिक व्यक्तियों को केवल सहानुभूति की नहीं, बल्कि स्वीकृति और उचित सहायता की ज़रूरत है। उनकी देखभाल केवल परिवार या डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देना चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि ऑटिस्टिक व्यक्ति भी उतने ही सक्षम और महत्वपूर्ण हैं जितने कि अन्य लोग। सही प्रशिक्षण, शिक्षा और सहयोग से वे समाज का अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए, हमें जागरूकता बढ़ानी होगी, पूर्वाग्रहों को दूर करना होगा और एक समावेशी वातावरण तैयार करना होगा, जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिले।