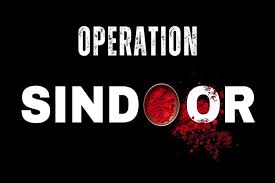भारत में इंडियन जूडिशल सिस्टम का नाम भी लेना इंडियन जूडिशल सिस्टम के लिए ऑफनसिव हो जाता है लेकिन उसी सिस्टम में बैठे सभी माननीयों की भाषा कैसी है एक बार मैं उस बार आपका ध्यान खींचना चाहूँगा…”बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा खतरनाक होते हैं।” “किसी महिला के ब्रेस्ट को छुना, उसके पाजामे का नाड़ा तोड़ना… बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।” ये मात्र दो उदाहरण हैं लेकिन ऐसे अनगिनत उदाहरणा यहां लिखे जा सकते हैं जिसमें हमारी न्यायपालिका के सबसे प्रमुख स्तंभ ने न्यायालय और सामाजिक की गरिमा की खुद ही धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सवाल है जब न्यायालय से भी ऊलजलूल फैसले और बयान आने लगे तो उन पर सवाल कौन और कैसे उठायेगा?
ज़वाब तो हमारे पास नहीं लेकिन कुछ तरीके है जिससे न्यायपालिका में आत्म-जवाबदेही को मजबूत किया जा सकता है।
भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन यदि आत्म-जवाबदेही मजबूत न हो, तो यही स्वतंत्रता न्यायिक निरंकुशता में बदल सकती है। आत्म-जवाबदेही का अभाव न्यायिक फैसलों की पारदर्शिता, निष्पक्षता और आम नागरिकों के विश्वास को प्रभावित करता है। इसे मजबूत करने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जा सकते हैं जैसे – न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और बाहरी निगरानी। वर्तमान में भारत में कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, जिसमें न्यायपालिका ही खुद के जजों का चयन करती है। इससे Conflict of Interest और परिवारवाद की आशंका बनी रहती है।
इसे बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसा कोई संगठन बनाना चाहिए जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हों। इससे नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
दूसरा मसला है, वर्तमान में न्यायाधीशों के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र न्यायिक लोकपाल की जरूरत। एक ऐसे संगठन का गठन किया जाना चाहिए, जो न्यायपालिका से स्वतंत्र हो और जिसमें रिटायर्ड न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी हो। यह लोकपाल शिकायतों की सुनवाई कर सके और यदि कोई जज दोषी पाया जाए तो उसे हटाने की सिफारिश कर सके।
इसके अलावा जो विचार करने वाली बात है कि कोर्ट की कार्यवाही अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है, जिससे आम नागरिकों को फैसलों की प्रक्रिया समझने का अवसर नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जनता यह देख सके कि न्यायाधीश किस आधार पर निर्णय लेते हैं। कोर्ट के फैसलों की विस्तृत व्याख्या आम भाषा में वेबसाइटों और सरकारी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाए।
भारत में न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार, पक्षपात या अनुशासनहीनता का कोई कठोर कानून भी नहीं है। एक नया न्यायिक जवाबदेही कानून बनाया जाए, जिसमें यह प्रावधान हो कि यदि कोई जज फैसलों में जानबूझकर पक्षपात करता है, तो उसे लोक सेवा नियमों के तहत दंडित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने की बाध्यता नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। ऐसे में सभी न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति और वित्तीय लेन-देन का सार्वजनिक खुलासा करना अनिवार्य किया जाना चाहिये, जिसे कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी रेगुलेट कर सके।
न्यायिक जवाबदेही का एक पहलू यह भी है कि मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो। लाखों केस लंबित रहने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। इसके लिए हर केस के निपटारे के लिए अधिकतम समयसीमा तय की जानी चाहिए।
जजों के लिए भी Performance Review System होना चाहिए। अभी जजों के प्रदर्शन की कोई स्वतंत्र समीक्षा प्रणाली नहीं है। ऐसा रिव्यू सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी निष्पक्षता, लंबित मामलों की संख्या, निर्णयों की गुणवत्ता और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को जांचा जाए और पॉइंट्स दिए जायें।
वर्तमान न्यायिक आचार संहिता में कई खामियां हैं, और इसका उल्लंघन करने पर जजों को कोई गंभीर दंड नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की जाए। यदि कोई न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो कोई स्वतंत्र अनुशासन समिति उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी प्रभावी हो सकती है, जब वह आत्म-जवाबदेही के दायरे में रहे। न्यायपालिका को पूरी तरह कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसे जनता और कानून के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए ठोस सुधार जरूरी हैं। पारदर्शिता, निगरानी तंत्र, सख्त कानून और न्यायाधीशों के कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन इन सभी उपायों को अपनाकर ही भारत में एक उत्तरदायी, पारदर्शी और निष्पक्ष न्यायपालिका का निर्माण किया जा सकता है।