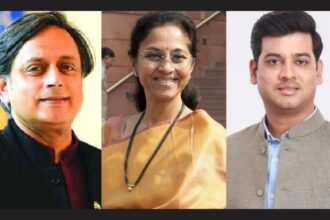जब भी भारतीय सिनेमा में देशभक्ति की बात होती है, तो कुछ नाम बिना कहे ज़हन में उभर आते हैं, उनमें सबसे पहला नाम मनोज कुमार का होता है। वे केवल अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक सोच, एक आदर्श, एक आंदोलन थे, जो परदे पर देश को जीते थे। उनका सिनेमा भारत की मिट्टी से निकला, और सीधे दिलों में उतर गया। वे उस सिनेमाई दौर के आख़िरी चेहरा थे, जिसमें देश पहले आता था और स्क्रिप्ट बाद में।
मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद (अब पाकिस्तान) में हुआ था। विभाजन के दौरान उनका परिवार दिल्ली आ बसा, जहां उन्होंने कठिनाइयों के बीच पढ़ाई की। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी था। पर जिस लड़के ने किशोरावस्था में दिलीप कुमार की फिल्मों को देखकर अभिनय का सपना देखा, उसने खुद को ही एक किरदार की तरह ढाल लिया और अपना नाम रखा…मनोज कुमार।
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फ़िल्मों की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती संघर्ष वही थे जो हर कलाकार के हिस्से आते हैं, छोटे रोल, रिजेक्शन, आर्थिक तंगी। लेकिन उनके भीतर जो जिद थी, वो साधारण नहीं थी। वह एक कलाकार की भूख नहीं, एक सिपाही की प्रतिबद्धता थी।
उन्हें असली पहचान मिली 1965 में आई फिल्म ‘शहीद’ से, जिसमें उन्होंने भगत सिंह की भूमिका निभाई। यह महज एक किरदार नहीं था…यह क्रांति की लौ थी, जो परदे से बाहर आकर दर्शकों की नसों में उतर गई।
इसके बाद मनोज कुमार ने न सिर्फ अभिनय किया, बल्कि लेखक और निर्देशक के रूप में भी खुद को साबित किया। और यहीं से शुरू होती है एक नई पहचान…‘भारत कुमार’!
1967 में आई फिल्म ‘उपकार’ ने उन्हें वो मुकाम दिया जिसे कोई पुरस्कार नहीं दे सकता जनता का विश्वास, देश का प्रेम। ‘जय जवान, जय किसान’ को सिनेमाई रूप में जीवंत कर देने वाली यह फिल्म आज भी ग्रामीण भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। एक भाई सैनिक बनकर सीमा की रक्षा करता है, दूसरा किसान बनकर खेत की। इस फिल्म में मनोज कुमार ने अभिनय, लेखन और निर्देशन…तीनों ज़िम्मेदारियाँ संभालीं।
इसके बाद ‘पूरब और पश्चिम’, ‘रोटी कपड़ा और मकान’, ‘क्रांति’, जैसी फिल्मों ने उन्हें और मज़बूती से देशभक्ति की धुरी पर स्थापित कर दिया। ये फिल्में केवल कहानियां नहीं थीं, ये विचार थीं, घोषणाएं थीं, जो सिनेमा के माध्यम से देश को झकझोर रही थीं।
मनोज कुमार का सिनेमा वैचारिक था। वह मनोरंजन करते हुए भी मूल्यों की बात करता था। उनके नायकों की लड़ाई सिर्फ खलनायकों से नहीं, समाज की विषमताओं, गरीबी, बेरोज़गारी, और नैतिक पतन से होती थी। उनके लिए सिनेमा समाज को आईना दिखाने का माध्यम था, न कि केवल टिकट बेचने की मशीन।
उन्होंने भव्यता के बिना भी भव्य सिनेमा बनाया। न गानों में फूहड़ता थी, न संवादों में चीख-चिल्लाहट। उनका संवाद—‘मैं एक आम आदमी हूं’…आज भी हमारी सड़कों, चाय की दुकानों और राजनीतिक भाषणों में गूंजता है।
मनोज कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री (1992) से सम्मानित किया गया। 2015 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। पर शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान वह उपनाम था जो जनता ने उन्हें दिया…भारत कुमार। यह कोई फिल्मी प्रचार नहीं था, यह जनता के दिल से निकला हुआ सलाम था।
जैसे-जैसे सिनेमा बदला, मानवीय मूल्य पीछे छूटने लगे। मनोज कुमार धीरे-धीरे फिल्मों से दूर हो गए। उन्हें समय से पहले ‘पुराना’ कह दिया गया। पर जो मूल्य उन्होंने अपने सिनेमा में गढ़े थे, वो आज भी किताबों, पाठ्यक्रमों और संविधान की आत्मा में जिंदा हैं।
अंतिम वर्षों में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली, लेकिन हर गणतंत्र दिवस, हर स्वतंत्रता दिवस पर जब कोई बच्चा ‘मेरे देश की धरती’ गाता है, तो कहीं न कहीं, उनकी आत्मा मुस्कुराती होगी।
आज जब हम सिनेमा को केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, तब मनोज कुमार जैसे कलाकारों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक फिल्म भी एक आंदोलन हो सकती है। उन्होंने साबित किया कि अभिनय केवल कला नहीं, एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है।
मनोज कुमार की जीवन-कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा कलाकार वही होता है जो अपने समय का दस्तावेज़ बन जाए। और उन्होंने अपने दौर को न सिर्फ जिया, बल्कि उसे परदे पर अमर कर दिया।
“वो परदे पर भारत बनकर जिए,
और परदे के बाहर भी भारत ही रहे।
मनोज कुमार सचमुच, एक जीवित भारत थे।”